दृश्य कला के मूलभूत दृश्य तत्व (Elements of Visual Arts)
ग्राफिक डिजाइन एक व्यवस्थित योजनाबद्ध संयोजन होता है जिसमें पाठकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन में प्रयुक्त वस्तु के चित्र ग्राफिक डिजाइन के मूल तत्वो (मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, व्यापारिक चिन्ह एवं कॉपी मैटर आदि ) को दृश्य कला के तत्वों के सुनियोजित संयोजन द्वारा डिजाइन में वास्तविकता का आभास कराया जाता है जिसमें वह डिजाइन आकर्षक एवं प्रभावशाली बनता है ! दृश्य कला के मूलभूत दृश्य तत्व निम्न प्रकार है -
1. रेखा (Line)
2. रंग (Colour)
3. आकृति / रूप (Shape/Form)
4. तान (Tone)
5. पोत (Texture)
6. अंतराल (Space)
1. रेखा (Line) -
रेखा दृश्य अभिव्यक्तिक का सरल, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माध्यम है ! दृश्य सम्प्रेक्षण का प्राथमिक साधन है ! रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो विचारों को अभीलिखित करने एवं प्रतीकात्मक बनाने तथा हमारे व्यक्तिगत तथ्यों एवं एहसासों को व्यक्त करने का मूल आधार होती है ! रेखाचित्र का विशेष गुण है, इसके अभाव में किसी की भी आकार की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है ! एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्तार रेखा कहलाता है और एक वर्णीय रेखाओं वर्ण्य वर्ण्य रेखाओं द्वारा किए गए अंकन, रेखांकन (Drawing) कहलाते हैं ! दृश्य कला में रेखाओं को गति के पथ के रूप से माना जा सकता है डिजाइन में रेखाएं पाठक की आंखों का मार्गदर्शन एवं मनोभाव भी को स्थापित करती है ! इन्हे निर्देशात्मक (Directional Lines) रेखाएं कहा जाता है यह रेखाएं डिजाइन या चित्र को देखने के लिए दृष्टि संचालन को निर्देशित करती है जिनके सहारे देखने वाले की आंखें डिजाइन के विभिन्न तत्वों के महत्व के अनुसार संचालित होती हैं ! डिजाइन में रेखाएं दृश्यरूप या अदृश्य रूप में भी हो सकती हैं ! दृश्य रूप की रेखाओं की चित्रित की गई रेखाएं या वर्णनात्मक रेखाओं (Descriptive Lines) के रूप में जाना जाता है ! यह रेखाएं डिजाइन या चित्र की विषय - वस्तु की भौतिक प्रकृति की जानकारी देती है और उनके आस - पास के स्थान का भी वर्णन करती है ! डिजाइन के किसी भी तत्वों का स्वरूप रेखाओं द्वारा ही दिखाई देता है ! चित्र या डिजाइन में दृश्य रेखाओं के अतिरिक्त अदृश्य रेखाएं भी होती है जिन्हें अंतर्निहित रेखाएं (Implied Lines) कहा जाता है ! यह रेखाएं डिजाइन या चित्र में भौतिक रूप से सृजित नहीं की जाती हैं बल्कि डिजाइनर या चित्रकार द्वारा संकेतिक रूप से सुझाई जाती है जिनके द्वारा देखने वाले की आंखें डिजाइन या चित्र के संदेश को क्रमानुसार जानने की कोशिश करती हैं ! डिजाइन में शीर्षक, उपशीर्षक, बॉडी कॉपी एवं चित्र को एक व्यवस्थित तरीके से एक सीध में रखने से भी अदृश्य रेखाओं का आभास होता है !
प्रत्येक रेखा का अपना प्रभाव होता है और वह डिजाइन में अर्थ और प्रभाव का सृजन करती है जिसे रेखाओं की अभिव्यक्तिक (Expressive) विशेषताएं कहां गया है जो रेखाओं के आकार, गति एवं धरातल पर बनाई गई रेखाओं के तरीके द्वारा निर्धारित की जाती है ! रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे - लंबवत या खड़ी रेखा (Vertical Line),अक्षतिज या आधारवत रेखा (Horizontal Line), तिरछी या कर्णवत रेखा (Diagonal Line), कोणीय रेखा (Angular Line), एक पुँजिय रेखा (Radial Line), चक्राकार रेखा (Spiral Line), प्रवाही रेखा (Rythamical Line), समकोणआत्मक रेखा (Right Angular Line), सख्त रेखा (Hard Line), सौम्य रेखा (Soft Line), अनियमित रेखा (Irregular Line), एवं टूटी - फूटी रेखा (Regged Line) आदि ! सभी रेखाओं का प्रभाव भी अलग अलग होता है ! जैसे -
(i) लंबवत या खड़ी रेखा (Vertical Line) - सामान्यतः गौरव (Dignity), दृढ़ता (Strength), उच्चता (Excellence), संतुलन (Balance), प्रतिष्ठा (Prestige), एवं महत्त्वआकांक्षा
(Ambitions) का भाव प्रकट करती है !
(ii) अक्षतिज या आधारवत रेखा (Horizontal Line) - स्थिरता (Stability), शांति (Peace), विस्तार (Expension) एवं निष्क्रियता (Inactivity) का भाव व्यक्त करती है !
(iii) तिरछी या कर्णवत रेखा (Diagonal Line) - ओजस्विता (Brilliance), गति (Speed), व्याकुलता (Agitation) का भाव होता है !
(iv) चक्राकार रेखा (Spiral Line) - लयपूर्ण गति (Rythamical Speed) एवं भ्रम (Confusion) को व्यक्त करती है !
(v) एक पुँजिय रेखा (Radial Line) - शक्ति (Power), शोभा (Grace)एवं प्रसार (Expension) का भाव व्यक्त करती है !
(vi) कोणीय रेखा (Angular Line) - तीव्रता (Intencity), संघर्ष (Struggle) एवं व्याकुलता (Agitation) का भाव रखती हैं !
(vii) प्रवाही रेखा (Rythamical Line) - मंद गति के साथ निरंतर प्रवाह को अभिव्यक्त करती हैं !
2. रंग (Colour)
रंग ( वर्ण ) दृश्य कला का महत्वपूर्ण तत्व होता है ! रंग प्रकाश का गुण है इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है यह अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क के ऊपर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है ! प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ती हैं तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अपने में सोख लेती हैं और कुछ को पुन: परावर्तित करती हैं ! यह परावर्तित प्रकाश ही उस वस्तु का रंग होता है जो हमारे अक्षपटल पर पड़ता है और उसी से उस वस्तु के रंग की जानकारी हमें मिलती है जो रंग अनुभूति (Colour Preception) कहलाता है ! रंग अनुभूति ( बोध ) में वर्ण की तरंग गति का बहुत महत्व होता है ! तरंगों की लंबाई जितनी अधिक होगी, उसकी गति उतनी ही तेज होगी जिसके कारण उसने तेजी एवं ऊष्मा का आभास होगा ! प्रकाश के रंगों की तरंग की लंबाई को यहां दिए चार्ट द्वारा समझा जा सकता है !
उपयुक्त सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था ! सन 1660 में आइजक न्यूटन (Issac Newton) ने प्रकाश की किरणों को त्रिकोण शीशा (Prism) के अंदर से गुजारा तो देखा कि यह प्रकाश विभिन्न सात रंगों (VIBGYOR) - बैंगनी (Voilet), आसमानी (Indigo), नीला (Blue), हरा (Green), पीला (Yellow), नारंगी (Orange) और
लाल (Red) विभाजित हो गया !
इस सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं और सभी रंगों के मिश्रण से सफेद प्रकाश का निर्माण होता है ! लाल, हरा और नीला रंग प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं ! इन्हें योगात्मक प्राथमिक (Additive Primary) कहां जाता है क्योंकि इन तीनों रंगों के योग से सफेद प्रकाश का प्रभाव बनता है ! इन तीनों योगात्मक प्राथमिक रंगों में से किन्ही दो की प्रकाश किरणों के मिश्रण से अन्य रंग बनते ( दिखाई ) देते हैं ! जैसे - लाल + नीला = मजेंटा (गुलाबी लाल ), हरा+ लाल = पीला एवं हरा + नीला = श्यान ( आसमानी नीला ) ! ये मजेंटा ( लाल ) पीला एवं श्यान ( आसमानी नीला ) रंग व्यवकलनात्मक प्राथमिक (Subtractive Primary) कहलाता है ! जो रंग रंग - द्रव्य (Pigments) की प्राथमिक रंगत होते हैं ! इन तीनों रंगों के द्रव्यों को मिश्रित करने पर गहरा रंग ( लगभग काला ) बनता है जो प्रकाश के परावर्तन (Reflection) को कम करता है ! इसलिए इन्हें व्यवकलनात्मक प्राथमिक रंग कहा जाता है ! इन तीनों प्राथमिक रंगों नीला, लाल व पीला (CMY) को अलग-अलग अनुपात में मिश्रित करने पर लगभग सभी रंग बनाए जा सकते हैं ! पूर्ण रंग की मुद्रण प्रक्रिया में इन्हें CMYK अथवा प्रोसेस रंग (Process Colour) के नाम से पहचाना जाता है ! प्रकाश के प्राथमिक रंगों का प्रयोग रंगीन चित्रों के रंग - विभाजन के लिए तथा रंगो - द्रव्य के प्राथमिक रंगों का प्रयोग मुद्रण एवं चित्रण के लिए किया जाता है !
कला सृजन में चित्रकारों एवं डिजाइनरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले रंग द्रव्य या पदार्थ (Pigments) के रंग कहलाते हैं ! प्राचीन ग्रंथ 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' ने पांच प्रकार के रंगों ( श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील ) का वर्णन मिलता है ! 'नाट्यशास्त्र' में श्वेत, लाल, नील और पीत मुख्य वर्ण माने जाते हैं ! वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण कला जगत में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है -
प्राथमिक रंग (Primary Colour) - लाल (Red), नीला (Blue) एवं पीला (Yellow) मूल प्राथमिक रंग है ! ये वे रंग होते हैं जो शुद्ध होते हैं, अर्थात किसी मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं !
द्वितीयक रंग (Secondary Colour) - प्राथमिक रंगों के किन्ही दो रंगों का मिश्रण करने से बनने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहा जाता है, जैसे - पीला + लाल = संतरी (Orange), पीला + नीला = हरा (Green), लाल + नीला = बैंगनी (Purple) ! इस प्रकार संतरी हरा और बैंगनी द्वितीयक रंग है !
तृतीयक रंग (Tertiary Colour) - द्वितीयक रंग में नजदीकी प्राथमिक रंग मिश्रित करने से जो रंग बनता है वह तृतीयक रंग (Tertiary Colour) कहलाता है ! जैसे - पीला + संतरी = तृणमणि (Amber), लाल + संतरी = सिंदूरी (Vermillion), लाल + बैंगनी = मजेंटा (Magenta), नीला + बैंगनी = नीला बैंगनी (Voilet), नीला + हरा = नील हरित (Aqua) एवं पीला + हरा = पीत हरित (Limegreen) ! श्याम और श्वेत ( काला और सफेद ) को तटस्थ रंग कहा जाता है !
उष्ण एवं शीत रंग (Warm and Cool Colour)
हमारे मन की भावनाओं के साथ रंगों का गहरा संबंध होता है ! भावनाओं के आधार पर ही हम रंगों को पसंद या नापसंद करते है ! रंगों की अनुभूति मानसिक प्रतिक्रिया पैदा करती है जैसे - नीला व हरा रंग ठंडक का एहसास कराते है ! लाल और संतरी गर्मी का एहसास कराते हैं ! इस मानसिक प्रतिक्रिया के आधार पर रंगों को ठंडे व उष्ण ( गरम ) रंगों में विभाजित किया जाता है ! हरा, नीला, बैंगनी एवं इनसे बनने वाली रंगते ठंडे रंग माने जाते हैं तथा लाल, पीला, सन्तरी और इनसे बनने वाली रंगते को गर्म रंग माना जाता है ! प्रत्येक रंग ( वर्ण ) में तीन भौतिक गुण होते हैं -
(i) वर्ण की रंगत (Hue),
(ii) वर्ण का मान ( Value ),
(iii) वर्ण की प्रबलता ( Saturation/Intensity/Chroma ) !
(i) रंगत : 'रंगत' रंग का वह नाम होता है जिससे हम एक रंग को पहचानते हैं ! जैसे - पीला, लाल, नीला आदि ! इन्ही रंगतो से विभिन्न रंगतो बनाई जाती है और वर्ण चक्कर रंगत के अनुसार ही व्यवस्थित किया जाता है !
(ii) मान : रंगत के गहरेपन और हल्केपन को रंग के मान के रूप रंग में जाना जाता है ! यह रंग का घनत्व होता है ! जब किसी श्याम - श्वेत छवियों को देखते हैं तो उसमें गहरा मान काले रंग के समीप होता है और हल्का मान सफेद रंग के समीप होता है और इन दोनों के मध्य में धूमिल (Gray) होता है यह गहरे से ग्रे में से होते हुए जो हल्की छवि बनाती है वह वर्ण का मान होता है ! रंग का जो मान सामान्य से कालेपन के समीप होता है वह छाया या गहरी रंगत (Shade) तथा जो मान सामान्य से सफेद के समीप होता है वह आभा या हल्की रंगत (Tint) कहलाता है ! रंग के मान के प्रभाव ( रंगत ) पर प्रकाश, वातावरण, दूरी एवं रंग के साथ पृष्ठभूमि में प्रयुक्त किए गए रंग कहा भी कहा भी प्रभाव होता है ! जैसे - एक धूमिल मान को काली पृष्ठभूमि में रखेंगे तो वह हल्का दिखाई देगा और यदि इसी धूमिल मान को सफेद पृष्ठभूमि में रखेंगे तो वह रंग का गहरा मान दिखाई देगा !
(iii) रंग की प्रबलता : यह रंग की शुद्धता और चमक का घोतक होता है जिसे रंग का बल भी कहा जाता है ! रंग की प्रबलता को कम करने के लिए या तो उस रंग में घुसर (Gray) मिलाकर या उस के पूरक रंग ( वह रंग वर्णचकर में उसके विपरीत होता है ) को मिलाकर रंग की प्रबलता को कम किया जा सकता है !
रंग सयोजना (Colour Combination)
डिजाइन या चित्र में प्रयुक्त प्रत्येक रंग दूसरे को प्रभावित करता है ! इसलिए रंग संयोजन में इनके एक दूसरे के प्रति सामजस्य एव विरोधाभास का ध्यान रखा जाता है जो वर्णचक्कर में
इनकी दूरी के आधार पर निर्भर करता है ! रंग संयोजन में मुख्यतः एक रंगीय योजना, (Monochromatic Scheme), सदृश रंग योजना (Analogues Scheme), पूरक रंग योजना
(Complementary Scheme), त्रयी योजना (Triad Scheme) एव वर्ण रहित योजना (Achromatic Scheme) का प्रयोग किया जाता है !
जब एक रंग की विभिन्न मान एवं प्रबलता का प्रयोग किया जाता है तो वह एक रंगीय योजना कहलाती है ! वर्णचक्कर में एक दूसरे के साथ वाले रंगों जैसे - ( नीला, हरा ) का प्रयोग किया जाता है तो वह सदृश या सहधर्मी रंग योजना कहलाती है, इसके विपरीत जब वर्णचक्कर से एक - दूसरे के सामने स्थापित रंगो ( किन्ही दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाला द्वितीयक रंग शेष बचे प्राथमिक रंग का विरोधाभासी या पूरक होता है ) का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो वह विरोधाभासी रंग योजना कहलाती है, जैसे हरा और लाल विरोधाभास या पूरक रंग है ! इसी प्रकार जब वर्णचक्कर के तीनों प्राथमिक रंगों ( लाल, नीला पीला ) का प्रयोग एक दूसरे के सान्निधय में किया जाता है तो वह त्रियी रंग योजना कहलाती है ! चित्र या डिजाइन बनाते समय जब केवल श्याम ( काला ) एवं श्वेत ( सफेद ) रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है वह वर्ण रहीत रंग योजना कहलाती है !
रंगों का चयन (Choosing the Colours)
रंग दृश्यआत्मक अनुभूति का महत्वपूर्ण पक्ष होता है क्योंकि रंग का दृश्य आकर्षण बहुत अधिक होता है ! वस्तुओं को श्याम - श्वेत की अपेक्षा रंगो के रूप में देखने व पहचानने में सरलता रहती है ! रंग डिजाइन व चित्र में उत्पाद की विशिष्टता, कॉपी के महत्व और डिजाइन के प्रति मनोदशा को स्थापित करता है और डिजाइन में ध्यानाकर्षण की क्षमता को बढ़ाता है ! माना जाता है कि रंगीन डिज़ाइन श्याम श्वेत की अपेक्षा 15 गुना अधिक प्रभावशाली होते हैं ! रंगों का भी प्रतीकात्मक अर्थ एवं मनोविज्ञान (Psychology) होता है जो डिजाइन के लिए बहुत ही महत्व रखता है ! जैसे -
(i) लाल रंग सबसे आकर्षक एवं तीव्र दिखने वाला होता है यह उत्तेजना एवं उग्रता (Excitement and aggression), वीरता (Bravery), क्रोध (Anger), प्यार (Love) एवं श्रृंगार (Beauty) को व्यक्त करता है !
(ii) नीला रंग इमानदारी (Honesty), निष्क्रियता (Inactivity), आशा (Expectation) एवं विस्तार (Expansion) का घोतक है !
(iii) हरा रंग प्रकृति (Nature), शांत (Cool), सुरक्षा (Safety) विश्राम (Ralex) एवं यौवन का घोतक होता है !
(iv) पीला रंग आशावाद (Optimism), प्रसन्नता (Festivity), प्रकाश (Light), बुद्धिमता (Wisdom), वर्धन (Growth) एवं दिव्यता (Divinity) का प्रतीक माना जाता है !
(v) सफेद रंग शुद्धता (Purity), पवित्रता (Holiness), सत्य (Truth), और शांति (Peace) का प्रतीक माना जाता है !
(vi) काला रंग गंभीरता (Seriousness), अवसाद (Depression) अंधेरे (Darkness), वर्धन (Growth) एवं डर (Fear) का प्रभाव पैदा करता है !
(vii) बैंगनी रंग राजसी (Royalty), रहस्य (Mystery), सम्मान (Dignity) एवं मृत्यु (Death) का प्रभाव पैदा करता है !
(viii) संतरी रंग वीरता (Bravery), ज्ञान (Knowledge), प्रेरणा (Stimulation) का प्रतीक माना जाता है !
डिजाइन निर्माण में रंगों के चुनाव में उपभोक्ता की मनोवृति बहुत महत्व रखती है ! रंगों के चयन में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रतिबिंबित होने चाहिए -
(i) उपभोक्ता की रूपरेखा और रंग के प्रति उसकी अभिरुचि,
(ii) रंग के साथ उपभोक्ता का सांस्कृतिक जुड़ाव,
(iii) प्रतिनिधियों करने वाली कंपनी की प्रतिष्ठा एवं विशेषता,
(iv) डिज़ाइनर का रंग के प्रति व्यक्तिगत लगाव,
(v) वर्तमान में रंगों के प्रति चलने वाला झुकाव आदि !
3. आकृति (Shape)
सामान्यत: वस्तु की आकृति को रूप कहा जाता है ! लेकिन मूल रूप में दिव आयामी धरातल की भाह्य रेखा आकृति और त्रिआयामी वस्तु की बाह्य सीमाएं रूप (Form) कहलाती है ! एक त्रिआयामी क्षेत्र में बने रूप को पुंज (Mass) कहा जाता है ! दिव आयामी डिजाइन या चित्र में पुंज को अंतर्निहित किया जाता है अर्थात पुंज का आभार कराया जाता है , जिसके लिए परीरेखाओं (Counter line) के छाया - प्रकाश, परस्परव्यापन (Overlapping) एक रूप के एक से अधिक पार्श्व को दिखाने से पुंज का आभार कराया जाता है ! विचारों को दृश्य रूप में अभिव्यक्त करने से ही आकृति अथवा रूप का निर्माण होता है ! यह अंतराल में किसी वस्तु की भौतिक उपस्थिति का एहसास कराता है जो वस्तु का भाह्य रूपाकार होता है ! आकृति से ही वस्तु की पहचान होती है ! डिजाइन में इसे रेखाओ रंग, एवं तान द्वारा बनाया जाता है ! एक डिजाइन ने प्रतीकात्मक, अमूर्त एवं यथार्थवादी आकृति हो सकती है ! जब एक समतल धरातल पर चित्र बनाते हैं तो समानांतर रूप से उस निर्धारित स्थान में एक दूसरी आकृति का भी सृजन होता है जिसमें विषयगत आकृति को सकारात्मक छवि ( चित्र आकृति ) तथा पृष्ठभूमि क्षेत्र को नकारात्मक छवि ( धरातल आकृति ) के रूप में इंगित करते हैं ! कुछ चित्रों या डिज़ाइनो में धरातल आकृति और चित्र आकृति इस चतुराई से बनायी जाती हैं कि उनमें ऊंचाई का छोर निश्चित नहीं होता है इस प्रकार रेखाओं की तरह आकृतियाँ भी अंतर्निहित होती है जो अन्य आकृतियों के कारण दिखाई देती है न कि वास्तव में बनी हुई होती है ! डिजाइन में पाठक के ध्यान को रोकने के सामर्थ्य मैं आकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विशेषत: अपेक्षित आकृति के साथ अपेक्षित रंग का संयोजन डिजाइन में विशिष्ट प्रभाव बनाते हैं ! जिससे उस तत्वों का डिजाइन में महत्व बढ़ जाता है ! आकृति डिजाइन में गति का प्रभाव पैदा करती है यदि आकृति को योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए तो वह पाठक की आंखों को मार्गदर्शक की तरह डिजाइन के मुख्य दृश्य - बिंदु से अन्य बिंदु दृश्य - बिंदु ( तत्व ) की ओर ले जाती है और डिजाइन में दृष्टि संचलन बनता है दृष्टि में संतुलन बनता है ! प्रत्येक आकृति का अपना एक दृश्य भार होता है जैसे - बड़ी, विषम किनारों और गहरी तान की आकृति का दृश्यभार छोटी हल्की तान और सम किनारों वाली आकृतियों से अधिक होता है ! मूल रूप से आकृतियां दो प्रकार की होती हैं : नियमित तथा अनियमित ! नियमित आकृतियां चार प्रकार की होती हैं - वर्गाकार, आयताकार त्रिभुज और गोल ! अनियमित आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे :- पेड़ - पौधे, फुल - पत्ता, पत्थर, पहाड़, बादल आदि की आकृतियां ! रंग एव रेखाओ की तरह ही विभिन्न आकृतियों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं, यथा -
(i) आयताकार (Rectangle) आकृतियां स्थिरता (Stability), एकता (Unity) एवं शक्ति (Power) की घोतक होती है !
(ii) त्रिभुजाकार (Triangle) आकृति सुरक्षा (Safety), अशांति Disturbance), शास्वत (Permanance) एवं विकास (Growth) का भाव पैदा करती हैं !
(iii) गोलाकार (Circle) आकृति पूर्णता शांति सुरक्षा लावण्य एवं गति को पैदा करती हैं और इसे ब्रह्मांड के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है !
(iv) वर्गाकार (Square) आकृति नीरसता (Dullness), एवं स्थायित्व (Stability) का भाव पैदा करती हैं !
आकृति का आकार (Size) डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण होता है डिजाइन का आकार एवं डिजाइन में किसी एक तत्व का आकार दोनों में डिजाइन की प्रभावक्षमता के लिए महत्वपूर्ण होते है ! आकार डिजाइन के तत्व को महत्व प्रदान करता है जैसे - अगर डिजाइन के किसी तत्व को अधिक महत्व देना है तो अन्य तत्वों की अपेक्षा उसका आकार बड़ा बनाया जा सकता है ! लेकिन कभी-कभी ध्यानाकर्षण के लिए डिजाइन के किसी तत्वों के आकार को अनपेक्षित रूप से छोटा भी बनाया जा सकता है ! डिजाइन में कुछ आकृतियां सूचना प्रदान करती हैं तो कुछ सजावट का कार्य करती है जैसे - डिजाइन के तत्व सूचना देते हैं तो रिक्त स्थान, बॉर्डर, रंग आदि डिजाइन के आकर्षण को बढ़ाते हैं !
4. तान (Tone)
रंग के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है ! आकृति की सतह के रंग के ऊपर पड़ने वाली छाया व प्रकाश की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है ! इसलिए इसे मान एवं प्रकाश (Value and Light) भी कहा जाता है ! जो चित्र या डिजाइन के क्षेत्र के हल्के या गहरेपन से संबंधित होता है जिसे चित्र में रंग की विभिन्न तानों द्वारा चित्रित किया जाता है ! प्रत्येक रंगीन वस्तु पर सुबह से रात्रि तक विभिन्न मात्रा में प्रकाश पड़ता है जिससे रंग में प्रकाश की मात्रा के अनुसार तान का मान (Value) बदलता रहता है ! जब रंग की रंगत (Hue) को घटाया जाता है तो मान को आसानी से महसूस किया जा सकता है ! रंगीन चित्र का श्याम - श्वेत फोटोग्राफ रंग की रंगत को एक घूसर (Gray) की श्रेणी में बहुत गहरे से बहुत हल्के में परिवर्तित कर देता है ! चित्र या डिजाइन कि यह विविधता हमें चित्र के प्रकाश एवं दूरी के प्रभाव को समझने में सहायता करती है !
डिजाइन में तान बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह डिजाइन के किसी भी तत्वों को अन्य की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करती है ! तान प्रकाश (Light) से प्रभावित होती है इसलिए प्रकाश का डिजाइन या चित्र के तत्वों के रूप में चित्रित और नियंत्रित किया जा सकता है तथा प्रकाश को एक मध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ! वर्तमान में लेजर किरणों से आश्चर्यजनक आकृतियों एवं प्रभाव का सृजन किया जाता है जिसका उत्कृष्ट उदाहरण चीन में आयोजित ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत प्रकाशीय प्रस्तुतियां थी ! पुनर्जागरण काल में यूरोपीय चित्रकारों ने छाया - प्रकाश के प्रभाव की नई तकनीक 'क्यूरोस्कयूरो' (Chiaroscuro) का विकास किया जिससे द्वि - आयामी चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था ! इसमें प्रकाश आने वाली दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता था और कभी - कभी प्रकाश के स्त्रोत को भी चित्र का भाग बनाया जाता था !
चित्रकार को डिजाइनर प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करता है जो विभिन्न प्रभाव पैदा करते हैं ! जैसे - तेज प्रकाश उत्तेजित करता है तो संध्या का वातावरण शांति प्रदान करता है तथा अंधकार से कौतूहल व भय उत्पन्न होता है ! उपयुक्त प्रभाव को डिजाइन में लाने के लिए रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है ! समानत: डिजाइन के लिए इलस्ट्रेशन ( चित्र ) बनाने एवं छायांकन करते समय प्रकाश की मात्रा के अनुसार उस चित्र या छायांकन में तान के प्रयोग से आकर्षक प्रभाव बनाये जाते है जो डिजाइन में वंचित मनोभाव पैदा करते हैं ! तान को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है -
(i) छाया (Dark)
(ii) मध्यम (Middle)
(iii) प्रकाश (Light)
5. पोत (Texture)
किसी वस्तु के धरातल की बनावट के गुण को पोत कहा जाता है ! यह कलाकृति की ऊपरी सतह की गुणवत्ता होती है जो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे - चिकना धरातल, गीला एवं सूखा और खुदरा एवं मुलायम धरातल आदि ! दृश्य कला में पोत का उल्लेख सतह की गुणवताओ के कुशल प्रयोग या सतहों की गुणवताओ के दृश्य प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है ! सभी सतहों का अपना पोत होता है जिनको छूने से या दृश्य प्रभावों द्वारा महसूस किया जा सकता है ! पोत को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - (i) वास्तविक, (ii) सृजित ( बनाए हुए )
(i) वास्तविक - वास्तविक वह होते हैं जिन्हें वस्तु को छूकर महसूस किया जा सकता है जैसे - लकड़ी, पत्थर मिट्टी एवं धातु आदि के पोत !
(ii) सृजित ( बनाए हुए ) - बनाए गए पोत वे होते हैं जो समतल धरातल पर सृजित किए जाते हैं !
डिजाइनर या चित्रकार द्वारा वास्तविक और बनावटी दोनों प्रकार की पोत का सृजन किया जा सकता है ! त्रिआयामी कला में मूर्तिकार प्रयुक्त होने वाली सामग्री के वास्तविक पोत और उनके मध्य संबंधों का प्रयोग कर सकता है या धरातलो को परिष्कृत कर नई पोत सृजन कर सकता है ! डिजाइन में डिजाइन के तत्वों के दोहराव के द्वारा भी पोत का सृजन किया जाता है ! पोत के द्वारा डिजाइन के संतुलन व किसी भी तत्वों के महत्व को घटाया व बढ़ाया जा सकता है जैसे - डिजाइन में समान आकार की दो आकृतियों में किसी एक को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसमें पोत डालकर उसके दृश्य - भार को बढ़ाकर उसे अधिक महत्व प्रदान किया जा सकता है और दृश्य - संतुलन को बनाया जा सकता है !
6. अंतराल (Space)
चित्र रचना के लिए रिक्तस्थान को अंतराल के नाम से जाना जाता है ! यह एक स्पर्शागम्य (Intangible) तत्व है जो निरंतर, असीम और सदैव विधमान रहता है ! 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' में इसे स्थान कहा गया है ! इस स्थान पर जैसे ही रेखा, रंग एवं पोत आदि द्वारा रूपाकृति का निर्माण होता है तो वह सजीव व सक्रिय हो जाता है ! डिजाइन में अंतराल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ! डिजाइन बनाने के लिए निर्धारित द्वि - आयामी चित्रभूमि एवं इस चित्रभूमि का डिजाइन की आवश्यकतानुसार व्यवस्थित रूप से उपयोग अंतराल विभाजन कहलाता है अर्थात अंतराल डिजाइन का वह तत्व या रूपाकार है जिसमें डिजाइन के तत्वों को सयोजित किया जाता है ! डिजाइन के तत्वों के अंकन के पश्चात यह अंतराल सक्रिय और सहयोगी दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है ! डिजाइन समतल धरातल पर जब डिजाइन के तत्वों को बनाता है तो उस तत्व वाले भाग ( विषयगत आकृति ) को सकारात्मक अंतराल तथा पृष्ठभूमि क्षेत्र को नकारात्मक या सहयोगी अंतराल ( धरातल आकृति ) के रूप में इंगित करता है किया जाता है यह अंतराल डिजाइन के तत्वों की आकृति रंग एवं पोत आदि के दृश्य भार से प्रभावित होता है कभी-कभी डिजाइन या चित्र में सक्रिय एवं सहायक अंतराल का भेद करना भी कठिन होता है !
अंतराल विभाजन (Space Division) - डिजाइनर या चित्रकार डिजाइन के तत्वों को संयोजित करने या चित्र निर्माण के बारे में सोच - विचार करता है तो संयोजन के सिद्धांतों के अनुसार संयोजन के तत्वों को दृश्य रूप में अभिव्यक्त करने के लिए अंतराल का विभाजन करता है जो मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है (i) सम विभाजन (Formal Division), (ii) विषम विभाजन (Informal Division)!
सम विभाजन - इस प्रकार के विभाजन में समसंतुलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें डिजाइन या चित्र के तत्व का दृश्य - भार पूर्ण चित्रभूमि में समान रूप से केंद्र बिंदु से सभी तरफ रहता है !
विषम विभाजन - इस प्रकार के विभाजन में आधे भाग की दूसरे भाग में पुनरावृति न करके डिजाइनर या चित्रकार स्वतंत्र रूप से अपनी सृजन क्षमता के अनुसार अंतराल का विभाजन कर सकता है ! इस प्रकार के विभाजन अधिक मौलिकता और सृजनात्मकता का प्रभाव बनता है जो डिजाइन या चित्र को अधिक आकर्षक एवं गतिमान बनाने में सहायक होता है ! अंतराल द्वारा डिजाइन के किसी भी तत्वों के महत्व को घटाया या बढ़ाया जा सकता है ! अंतराल डिजाइन संदेश में सरलता, विशिष्टता खुलेपन और मूल्य बहुमूल्यता को व्यक्त कर सकता है ! जिससे डिजाइन के साधारण संदेश को भी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है ! जब भी किसी डिजाइन या कला कार्य को देखते हैं तो मुख्यतः प्रथम प्रभाव का संबंध उसके अंतराल से भी होता है जिसमें उसे देखने से संबंधित दूरी भी शामिल होती है जो उसे नजदीक खड़े होकर देखने या कभी-कभी उसके आस - पास को देखने के लिए दूर खड़े होकर देखने से उसको अधिक महत्व प्रदान करती है !


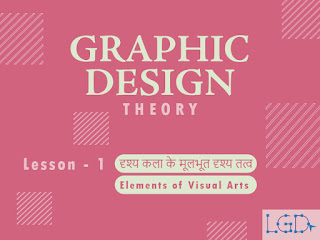


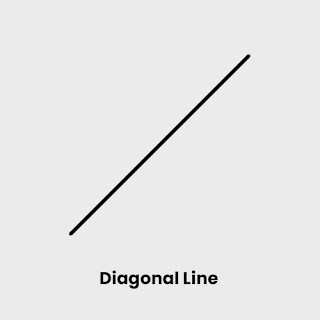



























0 Comments